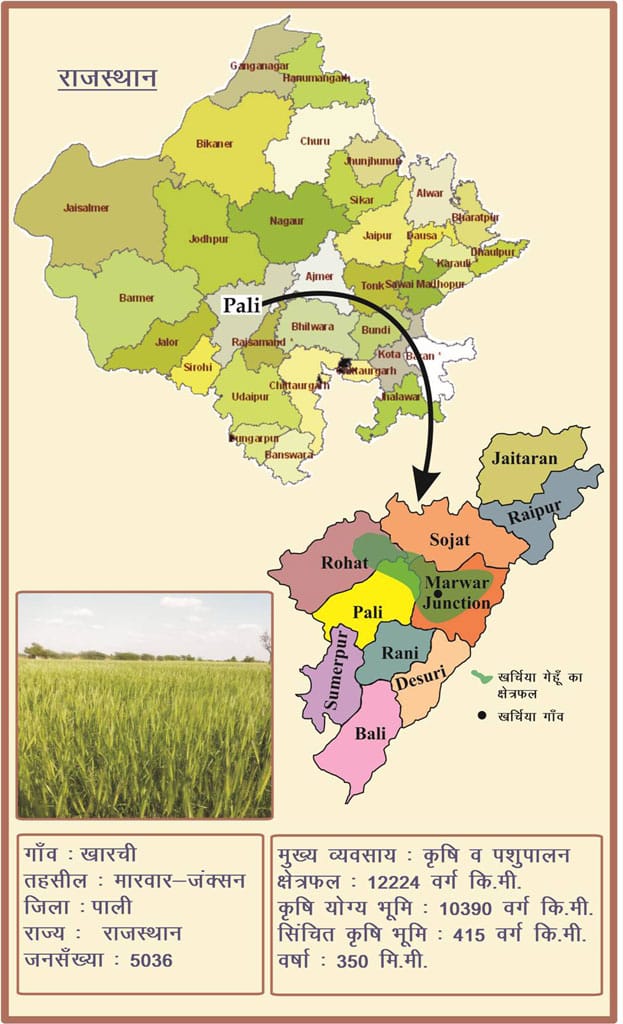इंडियन स्किमर्स: पानी की सतह को चीरता पनचीरा
पनचीरा कलाबाजी खाते हुए और करीने से पानी को चीरते हुए मछली का शिकार कर यह सिद्ध कर देता है की वह एक अचूक और माहिर शिकारी है और हर समय अद्वितीयरूप से विजित ही रहेगा, पर मानवीय हस्तक्षेप के चलते यह अपने एकमात्र प्रजनन स्थल या फिर यों कहे अपने अंतिम गढ़ चंबल नदी पर भी अस्तित्व की लड़ाई में पराजीत होता प्रतीत हो रहा है…
इंडियन स्कीमर (Indian skimmer) जिसे हिंदी में पनचीरा व राजस्थानी स्थानीय भाषा में पंछीडा भी कहते है। अपनी काली टोपी और चटक नारंगी रंग की चोंच, जिसका निचला भाग ऊपरी भाग की अपेक्षा लम्बा होने, के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका नाम, इसके भोजन को पकड़ने के तरीके से एक पल में ही स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यह अपनी चोंच से पानी की ऊपरी सतह को चीरते हुए, जैसे दूध से मलाई निकालते हो, मछली को पकड़ता है। इसका वैज्ञानिक नाम “Rynchops albicollis” है तथा यह Laridae परिवार का सदस्य है। यह कुछ हद तक टर्न (Tern) जैसे लगते है। राजस्थान में यह चम्बल व उसकी सहायक नदियों के पास मिलता है, परन्तु मानवीय हस्तक्षेपों और घटते आवास के कारण आज यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है।
इंडियन स्कीमर का चित्रण/निरूपण (Description):
इंडियन स्कीमर की चोंच उसके शरीर का सबसे आकर्षक भाग होती है क्योंकि इसकी चोंच लम्बी, मोटी, गहरी नारंगी तथा सिरे से हल्के पीले रंग की होती है। चोंच का निचला भाग ऊपरी भाग की अपेक्षा लम्बा होता है तथा यह सिरे से चाकू की तरह चपटा व धारदार होता है। इसके सिर का ऊपरी भाग काला होता है मानो सिर पर काली टोपी रखी हो। शरीर के ऊपरी भाग काले तथा निचले भाग सफ़ेद रंग के होते हैं। अपने लम्बे और नुकीले पंखों के कारण यह टर्न जैसा दिखता है परन्तु इसके पंखों के किनारे सफ़ेद होते है तथा इसके पंखों का विस्तार लगभग 108 सेमी होता है। इसकी पूँछ काली, छोटी, सिरे से कांटे जैसी तथा इसके बीच के पंख सफ़ेद होते है। टंगे तथा पैर लाल होते है। नर और मादा दिखने में एक से ही होते हैं, हालांकि, नर आकार में थोड़े बड़े होते हैं।
युवा पक्षियों के शरीर के ऊपरी भाग भूरे तथा सिर वयस्कों से ज्यादा सफ़ेद होता है। इनकी चोंच नारंगी-भूरी तथा सिरे से गहरे रंग की होती है। चोंच सामान्य ही होती है परन्तु उम्र के साथ निचला भाग बढ़ जाता है। एक नज़र में किसी उड़ान भरते या स्थिर बैठे स्कीमर को देखने पर उनकी क्षैतिज रूप से विस्तारित (horizontally extended) आँखें एक पतली पट्टी या धारी (slits) कि तरह दिखती हैं जो कि इनके समुद्र की सतह पर घूमते समय पानी के संभावित बौछार से आँखों को सुरक्षित रखता है।

इंडियन स्कीमर “Rynchops albicollis” (फोटो: डॉ. धर्मेंद्र खांडल)
इतिहास के पन्नो में इंडियन स्कीमर
इंडियन स्कीमर का जिक्र सबसे पहले एडवर्ड बक्ले (1602-1709) द्वारा बनाए गए उनके चित्र में किया गया। एडवर्ड बक्ले मद्रास में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्जन और एक अग्रणी प्रकृतिवादी थे। ये पहले इंसान थे जिन्होंने भारतीय पक्षियों की प्रजातियों के चित्र बनाकर दस्तावेजीकरण किया था। इन्होंने मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज (Fort St. George) के आसपास के इलाके से कुल 22 पक्षियों के चित्र व विवरण तैयार किए थे। सन 1713 में यह सभी विवरण और चित्र एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी जॉन रे की किताब Synopsis Methodica Avium & Piscium: Opus Posthumum में छपे जो कि भारतीय पक्षियों पर छपने वाला पहला दस्तावेज था। एडवर्ड बक्ले ने ही स्कीमर का सबसे पहला चित्र बनाया जिसे उस समय मद्रास सी क्रो (Madras Sea Crow) का नाम दिया था।
अल्फ्रेड हेनरी माइल्स ने An Encyclopedia of Natural History में जिक्र किया है कि सन 1731 किसी अमेरिकी लेखक ने समुद्र के ऊपर पानी को चीरते हुए उड़ने वाले पक्षी को “cut water” नाम से संबोधित किया था जो कि बाद में Scissors Bill नाम से जाना जाने लगा।
विलियम जॉन स्वेन्सन (William John Swainson) ने सन 1838 में इंडियन स्कीमर को द्विपदनाम पद्धति के अनुसार “Rynchops albicollis” नाम दिया। स्वेन्सन एक अंग्रेजी पक्षी विशेषज्ञ,मैलाकोलॉजिस्ट, किट विशेषज्ञ और कलाकार थे जो प्रकृति के सुंदर रंगीन चित्रों, विशेष रूप से फूलों और पक्षियों के लिए जाने जाते थे।

एडवर्ड बक्ले द्वारा बनाया गया मद्रास सी क्रो (Madras Sea Crow) का चित्र
इंडियन स्कीमर का वितरण
पक्षी विशेषज्ञ TC Jerdon द्वारा 1864 में भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक के एक विवरण कि कल्पना करें तो ये अनुमानित किया जा सकता है कि पनचिरा कभी हजारों कि तादाद में पाया जाता था। जेरडोन कि पुस्तक का विवरण कुछ इस प्रकार है “श्री ब्रुक्स लिखते है की उन्होंने मिर्ज़ापुर में सैकड़ों की तादाद में स्किमर्स के चूजे को देखा तो वो दृश्य आश्चर्यचकित कर देने वाला था, मानो बहुत सारे छोटे कछुए की सेना नदी की तरफ दौड़ रही हो।”
इंडियन स्कीमर मुख्य रूप से नदियों, झीलों और नमभूमियों में पाया जाता है। सुन्दर (2004) के अनुसार, पहले यह म्यांमार की प्रमुख नदियों, भारत-चीन में मेकांग के आसपास तथा भारतीय उप-महाद्वीप में व्यापक रूप से मिलते थे। परन्तु इसकी सीमाएं हाल के दशकों में तेजी से खंडित हुई है जिसके परिणामस्वरूप आज पाकिस्तान और म्यांमार में इनकी बहुत छोटी सी आबादी जीवित बची है तथा मेकांग डेल्टा में यह पूर्णरूप से लुप्त हो चुकी है। मोहसिन (2014) के अनुसार, वर्तमान में भारत, और बांग्लादेश इंडियन स्कीमर के अंतिम गढ़ हैं तथा भारत इस प्रजाति के लिए एकमात्र शेष प्रजनन आवास है। भारत में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा से इसकी सूचना है।

Distribution of Indian Skimmer (Source: birdlife.org)
आज भारत में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भारतीय स्किमर की एक बड़ी आबादी (लगभग 80 प्रतिशत) का प्रजनन स्थान है। अभी तक राजस्थान में यह केवल चम्बल व उसकी सहायक नदियों जैसे रामेश्वरम घाट, बनास नदी व इसके पास के कुछ तालाबों जैसे “सूरवाल” में देखा जाता है। इनको आसानी से चम्बल नदी के किनारे पर देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में इंडियन स्किमर (फोटो: डॉ. धर्मेंद्र खांडल)
आहार व्यवहार
इंडियन स्कीमर का नाम इसके भोजन के शिकार करने की विधि के आधार पर रखा गया है। यह अपनी चोंच को खोल कर पानी की सतह को निचली चोंच से चीरते हुए, सीधी उड़ान भरते है और जैसे ही कोई मछली सामने आती है तो तुरंत अपनी चोंच से उसे पकड़ लेते है। यह एक उल्लेखनीय एरोबैटिक कौशल दिखाते हैं जिसमें यह अपनी चोंच को पानी की सतह पर स्थिर एक सीधे पथ पर बनाये रखते है। यह देखा गया है की इंडियन स्कीमर मुख्यरूप से सतह पर उपलब्ध छोटी मछलियों की प्रजातियों को खाते है तथा छोटे झुंडों में खाना खोजते है। इसके आहार में मुख्य रूप से 04-14 सेमी लंबाई की छोटी मछलियाँ होती हैं तथा जो मछली 2 सेमी से छोटी होती है, उन्हें युवा पक्षियों को खिलाया जाता है। राजगुरु (2017) के अनुसार यह Salmophasia bacaila, Salmophasia sardinella, Systomous sarana, Pethiaticto, Dermogenys pusilla आदि प्रजातियों की मछलियां खाते है।

अपनी चोंच से पानी की सतह को चीरते हुए मछली पकड़ते इंडियन स्कीमर (फोटो: डॉ. धर्मेंद्र खांडल)
प्रजनन
इंडियन स्कीमर का प्रजनन काल भीषण गर्मी के दिनों में (मार्च से मई) होता है तथा यह मुख्य रूप से खुले रेत तट पर अपना घोंसला बनाते है। अंडे भूरे धब्बों और लकीरों के साथ सफेद व भूरे रंग के होते हैं। राजगुरु (2017) ने यह सूचित किया है की तेजी गर्मियों में यह अपने अंडों को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए बार-बार पानी में जाकर अपने अग्र भाग को भिगो कर अंडों पर बैठ उन्हें ठंडा करते है। देबाता (2018) ने यह सूचित किया है की इंडियन स्कीमर, टर्न के घोंसलों में अपने अंडे रख कर Brood Parasitism का उद्धरण देते है, परन्तु इस व्यवहार के अन्य संदर्भ नहीं आये है। इनका प्रजनन काल नदियों के जल स्तर पर भी निर्भर करता है।
इंडियन स्कीमर पर खतरे
पहले यह पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से मिलता था परन्तु आज मानवीय हस्तक्षेपों के चलते यह बहुत कम हो गए तथा IUCN के अनुसार एक संकटग्रस्त प्रजाति है। वर्तमान में इसकी वैश्विक आबादी केवल 6,000-10,000 पक्षी हैं। यह मनुष्यों द्वारा निवास स्थान के खत्म होने, मछली पकड़ने, परिवहन, घरेलू उपयोग, सिंचाई योजनाओं और कृषि व औद्योगिक रसायनों से नदियां व झीलें प्रदूषित हो रही है तथा इन्हीं कारणों से इंडियन स्कीमर की आबादी में गिरावट आ रही है क्योंकि इन कारकों ने इसके प्रजनन और खाना ढूंढने की सफलता को कम कर दिया है। सुंदर (2004) के अनुसार राजस्थान में चम्बल नदी के ऊपर बांध बनने से, भी इसकी आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बाँध से पानी छोड़ने के कारण जलस्तर में निरंतरता नहीं रहती है। प्रजनन काल में यह नदी किनारे रेत पर घोंसला बनाते है परन्तु ऐसे में यदि बाँध से पानी छोड़ा जाता है तो नदी किनारों पर जलस्तर बढ़ने के कारण इनके घोंसले बह जाते है। और यदि किनारों पर पानी बहुत काम रहे तो आवारा कुत्ते व मवेशी, इनके घोंसलों को नष्ट कर देते है।
इसकी अधिकांश आबादी असुरक्षित हैं लेकिन कुछ संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में सुरक्षित हो रही है। परन्तु सरकार को इस पक्षी के संरक्षण के लिए और कदम भी उठाने चाहिए, क्योंकि यह जल-पक्षी नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं तथा ये पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
References:
- Debata, S., T. Kar, K.K. Swain & H.S. Palei (2017). The Vulnerable Indian Skimmer Rynchops albicollis Swainson, 1838 (Aves: Charadriiformes: Laridae) breeding in Odisha, eastern India. Journal of Threatened Taxa 9(11): 10961–10963
- Debata, S., T. Kar, K.K. Swain & H.S. Palei(2018): Occurrenceof Indian Skimmer Rynchops albicollis eggs in River Tern Sterna aurantia nests, Bird Study
- https://books.google.co.in/books?id=DWtCw6-AxA8C&pg=PA262&lpg=PA262&dq=Indian+scissors-bill+name+given+by&source=bl&ots=gUvUYj5lrJ&sig=ACfU3U1FPmQ5xerPWDd8fDQwWPqpYK92DQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjvsoz4m_joAhWKzDgGHQ8ZB4YQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=Indian%20scissors-bill%20name%20given%20by&f=false
- Jerdon, TC (1864). Birds of India. Vol 3. George Wyman & Co. p. 847.
- John Ray & Edward Buckley. 1713. Synopsis methodica avium & piscium : opus posthumum, quod vivusrecensuit & perfecit ipse insignissimus author: in quo multas species, in ipsiusornithologiâ &ichthyologiadesideratas, adjecit: methodum quesuampiscium naturæ magìsconvenientemreddidit. Cum appendice, &ico. P.203
- Rajguru, S. K., (2017). Breeding biology of Indian Skimmer Rynchops albicollis at Mahanadi River, Odisha, India. Indian BIRDS 13 (1): 1–7.
- Sundar, K.S.G. (2004). Observations on breeding Indian Skimmers Rynchops albicollis in the National Chambal Sanctuary, Uttar Pradesh, India. Forktail 20: 89–90.
- Swainson,1838. Animals in menageries. Part III. Two centenaries and a quarter of birds, either new or hitherto imperfectly described. p. 360.